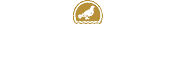मोदी सरकार ने सामान्य श्रेणी में आने वाली अगड़ी जातियों-समुदायों के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला ऐसे वक़्त लिया है, जब लोकसभा चुनाव महज तीन महीने दूर है. देश में बेरोज़गारी की दर 7.4 फीसदी है और बीते साल देश में कुल 1.1 करोड़ नौकरियां ख़त्म हुई है. इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि आज़ादी के बाद पहली बार कोई सरकार संविधान से इतर आरक्षण का एक नया फार्मूला सामने लायी है. अब तक एससी-एसटी और ओबीसी के सभी तरह के आरक्षण-प्रावधान समाधिक शौक्षिक पिछड़ेपन पर आधारित थे. संविधान ने इसी सिद्धांत पर भारत में सकारात्मक कार्यवाई का आधार तय किया था. पर केंद्र सरकार ने ७ जनवरी को संविधान के इस दर्शन को पलटते हुए सामान्य श्रेणी के लोगों को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण देने का एलान किया. इसमें अल्पसंख्यक समाजों कि सामान्य श्रेणी भी शामिल की गई है.
संघ और बीजेपी
चूकिं फैसला एक संविधानेत्तर धारणा पर आधारित है, इसलिए इसे लागू कराने के लिए सरकार संविधान के अनुछेद 15 और 16 में संशोधन कि पहल करेगी. सवाल उठता है कि क्या संविधान कि मूल संरचना और वैचारिक आधार के बाहर जाकर किया गया कोई संविधान संशोधन वैध होगा? आरक्षण का आधार आर्थिक हो या सामाजिक-शैक्षिक, संविधान सभा ने लंबी बहस के बाद यह विवाद हल कर लिया था. उस ऐतिहासिक फैसले को पलटने वाले किसी नए संविधान को संसद कि मंजूरी मिल भी गई तो क्या वह न्यायिक स्तर पर टिकेगा? सन 1973 में ‘केशवानंद भर्ती बनाम राज्य’ के मुक़दमे में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा था, ‘संसद को संविधान संशोधन का अधिकार है, पर संशोधन के नाम पर वह संविधान के बुनियादी विचार या संरचना को नहीं पलट सकती.’
मौजूदा सरकारी फैसले के तात्कालिक लक्ष्य के साथ इसका एक दूरगामी लक्ष्य भी नज़र आ रहा है. तात्कालिक लक्ष्य चुनावी समीकरण ठीक करना है. तीन प्रमुख हिन्दीभाषी राज्यों में बीजेपी कि चुनावी हार का कारण यह भी माना गया कि एससी-एसटी एक्ट मामले से नाराज़ हिन्दू अगड़ो के एक हिस्से ने उसे छोड़ कांग्रेस का साथ दिया है. इससे बीजेपी ने सबक लिया और लोकसभा चुनाव से पहले इस फैसले के जरिये हिन्दू अगड़ों को खुश करने कि कोशिश की है. वह अल्पसंख्यकों से ज़्यादा समर्थन की उम्मीद नहीं करती. पर इस तात्कालिक लक्ष्य के मुकाबले उसका दूरगामी लक्ष्य ज़्यादा वैचारिक और राष्ट्र-राज्य के लिए ज़्यादा घातक है. इसके जरिये संघ- बीजेपी ने संविधान के मूल चरित्र में क्रमश: बदलाव लाने की पहली बड़ी कोशिश की है.
बीते दो दशकों में संघ को समझ में आ गया है कि संविधान को एकबारगी नहीं बदला जा सकता. इसलिए वह क्रमश: इसके मूल चरित्र को बदलने में जुटा है. हमारे संविधान में आरक्षण का प्रावधान गरीबी उन्मूलन या समाजवाद लाने के लिए नहीं रखा गया. वह समाज-शासन में वंचित और पिछड़े समुदायों का प्रतिनिधत्व बढ़ाने के लिए रखा गया. इसे बदलने के लिए संविधान संशोधन होता है तो वह पहले के संशोधनों से बिलकुल अलग, संविधान के एक अहम् सिद्धांत को पलटने वाला होगा. इस फैसले का एक और पहलू संघ- बीजेपी कि अंदरूनी राजनीति से जुड़ा है. मोदी-शाह कि जोड़ी ने इसके जरिये संघ को खुश करने की कोशिश की है.
पिछले कुछ सालों से सरकार के कामकाज और जनता में उसकी लोकप्रियता से संघ नेतृत्व सत्ता की मौजूदा जोड़ी से कुछ ज़्यादा खुश नहीं था. संघ के अत्यंत विश्वासपात्र केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की हाला की तीखी टिप्पणियों को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है. कुछ अन्य संघ नेताओं ने भी सरकार पर तल्ख़ टिप्पणियां कीं. अब से साढ़े तीन साल पहले, बिहार विधान सभा चुनाव से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण नीति की विषाद समीक्षा का आह्वान किया था. तब लालू-नीतीश मिलकर चुनाव लड़ रहे थे. कुछ ही महीने पहले केंद्र की सत्ता में पूरी ताकत से आई बीजेपी के लिए बिहार में चुनाव जीतने की पूरी आशा थी. पर वह बुरी तरह हार गई. बीजेपी नेताओं ने हार का कारण भागवत के उस ब्यान को भी माना. भागवत का वह ब्यान आज ठीक से देखें तो नई आरक्षण पहल का राजनीतिक संदर्भ समझना आसान हो जाएगा. एक तरफ यह लोकसभा चुनाव से पहले पस्त पड़ी बीजेपी को फिर से सियासी ताकत देने की कोशिश है तो दूसरी तरफ संघ-वैचारिकी को अमली जामा पहनाने का बड़ा कदम भी है. ज़्यादातर दल और सामाजिक समूह संघ-बीजेपी के इस आरक्षण-आख्यान को सिर्फ अपने चुनावी चश्मे से देख रहे हैं. समाज में प्रभावशाली अगड़ी जातियों को नाराज़ करने का जोखिम वह नहीं लेना चाहते. यह सवाल भी वह ठीक से नहीं उठा पा रहे हैं कि अगड़ी जाति के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को फ़ायदा देना है तो आरक्षण का दायरा सिर्फ सरकारी क्षेत्र तक क्यों सीमित है, जहाँ नौकरियों कि सम्भावना ही नहीं है!