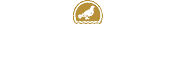कार्बन सिंक के रूप में, जैव विविधता के लिए रिपोजिटरी के रूप में, स्थानीय जलवायु नियंत्रण के लिए प्रभावी उपकरण के रूप में, और लकड़ी और संबंधित उपज के स्रोत के रूप में वनों को बहुत महत्व का ग्रह संसाधन माना जाता है। वन भी लोगों के लिए निवास स्थान रहे हैं। सतत विकास के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है कि वनों को संरक्षित किया जाए और भावी पीढ़ियों के लिए जैव विविधता का संरक्षण किया जाए। सतत विकास यह भी कहता है कि वर्तमान पीढ़ी इस प्रक्रिया में पीड़ित नहीं होती है। वर्तमान मांगों और भविष्य की सुरक्षा के बीच एक निरंतर तनाव है। भारत में सदियों से, जंगलों का उपयोग मानव द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा है – निवास स्थान से लेकर भोजन के भंडार से लेकर आजीविका के स्रोत तक। कहीं भी 100 मिलियन से 300 मिलियन लोगों के बीच, ज्यादातर जनजातियाँ, वनों में और उसके आसपास रहती हैं। थोड़ी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच के साथ वे गरीब और अल्पपोषित हैं। वे जीवित और आजीविका के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। वे हमेशा जंगलों के पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर सद्भाव में रहते हैं।
यह 19 वीं और 20 वीं शताब्दी के प्रारंभ में था कि अंग्रेज जंगलों को बंजर भूमि के रूप में मानने लगे थे, जिनका उपयोग वाणिज्यिक फसलों के कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जा सकता था। निर्यात के लिए जंगलों को लकड़ी के स्रोत के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रेलवे पटरियों के तेजी से विस्तार के दौरान रेलवे स्लीपरों में टिम्बर का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था। वन भूमि और संसाधनों पर औपनिवेशिक सरकार की पकड़ को मजबूत करने के लिए, 1927 का भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया था। इसके अनुसार, वनों की तीन श्रेणियां थीं: आरक्षित, संरक्षित और गाँव। आरक्षित वन को सरकार से संबंधित वन या बंजर भूमि के किसी भी मार्ग पर अधिसूचित किया जा सकता है। ऐसे जंगल में सरकार की अनुमति के बिना कुछ भी अनुमति नहीं थी। वन अधिकारी असली नियंत्रक बन गए। संरक्षित वनों को अधिसूचित क्षेत्र थे जहाँ पेड़, या पेड़ों का एक वर्ग और, बहुत बाद में, कुछ लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षित किया गया था। सरकार को स्थानीय समुदाय द्वारा उपयोग किए जाने वाले आरक्षित वन (आमतौर पर गांव से सटे) के एक हिस्से का उपयोग करने के लिए अधिकार देने की अनुमति दी गई थी। यह स्पष्ट था कि सरकार, वनभूमि ’बना सकती है, जरूरत के हिसाब से उसका दोहन कर सकती है, और मूल वनवासी अपनी ही भूमि में वन अधिकारी बनकर रह रहे हैं।
पिछले चार या पाँच दशकों में वनों के पर्यावरणीय मूल्य की बेहतर सराहना की जाने लगी, लेकिन संरक्षण पर लोग प्रवचन छोड़ते रहे। यदि कुछ भी हो, तो वनवासियों की प्रथाओं पर संदेह की दृष्टि से देखा गया। उनकी खेती और शिकार की प्रथाएं जंगलों को अस्थिर बना सकती थीं। वैकल्पिक रोजगार और नई आजीविका के बिना, वनवासियों को विकास के समाजवादी मॉडल और साथ ही नव-उदारवादी दोनों के बंधन से छोड़ दिया गया था।