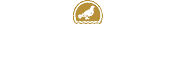जब टीएफआर 2.1 को छूता है, जिसे प्रतिस्थापन प्रजनन स्तर कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जनसंख्या स्थिर हो रही है, क्षणिक कारक के अधीन है। भारत की जनसंख्या 2060 में 1.7 बिलियन होने का अनुमान लगाया गया था, जो 2100 तक घटकर 1.5 बिलियन हो गई। एनएफएचएस की रिपोर्ट के अनुसार टीएफआर में तेजी से गिरावट बताती है कि ये भविष्यवाणी की तुलना में बहुत पहले हो सकते हैं। इस प्रकार, जनसांख्यिकीय रुझान के संदर्भ में घबराहट का कोई कारण नहीं है।
टीएफआर की गिरावट के लिए गर्भ निरोधकों की बढ़ती स्वीकार्यता सिर्फ एक कारक है। विभिन्न NFHS राउंड के डेटा विवाहित महिलाओं द्वारा गर्भनिरोधक प्रथाओं में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं दिखाते हैं। आधुनिक गर्भनिरोधक विधियों का उपयोग करने वाली महिलाओं का प्रतिशत भी बहुत अधिक नहीं बढ़ा है। यह 2005-6 और 2015-16 के बीच का मामला था – इस अवधि में टीएफआर में उच्च गिरावट दर्ज की गई। मुख्य कारक जो इस महत्वपूर्ण गिरावट का कारण बना वह है शादी की उम्र में वृद्धि।
एनएफएचएस 2015-16 रिकॉर्ड करता है कि 20-24 आयु वर्ग में विवाहित महिलाओं में, जो महिला गर्भवती थीं या 18 साल की उम्र से पहले या जिनके बच्चे थे, 2005-06 में 48 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 21 प्रतिशत हो गई। देश में यह जनसांख्यिकीय लाभ मुख्य रूप से पहले बच्चे के जन्म के समय वृद्धि के कारण है। गर्भनिरोधक उपयोग में कोई वृद्धि नहीं बताई जा रही है, यह आंशिक रूप से विवाह की आयु में वृद्धि के कारण होता है, क्योंकि युवा जोड़ों को इन तरीकों को चुनने की अधिक संभावना होती है।
टीएफआर में गिरावट से निर्भरता दर में कमी आएगी। बच्चों की हिस्सेदारी में कमी और वयस्क जनसंख्या में वृद्धि आर्थिक विकास की उच्च दर को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे कामकाजी आबादी के प्रतिशत में वृद्धि होगी। एशियाई विकास बैंक की भविष्यवाणियों के अनुसार, भारत को आने वाले तीन दशकों में कम से कम 6.5-7.5 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। यह रिकॉर्ड विकास काफी हद तक जनसांख्यिकीय लाभांश और अन्य संरचनात्मक कारकों, वर्तमान आर्थिक संकट के बावजूद प्राप्त किया जा सकता है।
भारत में उच्च आय वृद्धि का परिदृश्य गंभीर रूप से कार्य सहभागिता दर और कौशल विकास में वृद्धि पर निर्भर है। अनुमानित विकास दर को प्राप्त करने के लिए, कार्यबल में भाग लेने वाली महिलाओं के प्रतिशत में वृद्धि एक आवश्यक है। कामकाजी महिलाओं के प्रतिशत में गिरावट के बावजूद, टीएफआर में तेज गिरावट और शादी की उम्र में वृद्धि का रुझान बताता है कि यह संभव है। रोजगार कारणों से महिलाओं के प्रवास में तेज वृद्धि इस बात को और पुष्ट करती है।
मुस्लिम समुदाय के बीच गरीबी और अशिक्षा का उच्च स्तर अन्य समुदायों की तुलना में अपने बड़े “वांछित बच्चों की संख्या” की व्याख्या करता है। हालाँकि, स्थिति नाटकीय रूप से बदल रही है। 2005-6 में, मुसलमानों के लिए टीएफआर 3.4 था जो 2015-16 में गिरकर 0.8 प्रतिशत अंक तक गिर गया। हिंदुओं के लिए, टीएफआर 2005-06 में 2.6 से घटकर 2015-16 में 2.1 हो गया – 0.5 अंक की गिरावट। ईसाइयों और सिखों के लिए गिरावट केवल 0.3 प्रतिशत अंक थी।
इसका कारण शिक्षा की स्थिति में सुधार और आर्थिक विकास और आधुनिकता के लाभ हाशिए पर मौजूद समुदायों तक पहुंचना है। स्पष्ट रूप से, परिवार नियोजन के गैर-टर्मिनल और रिक्ति तरीकों की स्वीकृति मुस्लिम महिलाओं के बीच बढ़ी है, हालांकि नसबंदी जैसे टर्मिनल तरीके बहुत लोकप्रिय नहीं हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य और शिक्षा ने उनकी टीएफआर को नीचे लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के परिणामस्वरूप गिरावट सार्वभौमिक है, लेकिन प्रभाव मुस्लिम महिलाओं के लिए अधिक है, जैसा कि एनएफएचएस डेटा के माध्यम से पता चला है।
स्कूल में उपस्थिति की कम दर और मुस्लिमों द्वारा स्कूलों में बिताए कम साल गरीबी के कारण हैं, क्योंकि युवा लड़के बहुत जल्दी श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं। लड़कियाँ पारंपरिक और सांस्कृतिक कारकों के कारण स्कूलों से बाहर हो जाती हैं, इसके अलावा युवा भाई-बहनों की देखभाल करने की आवश्यकता होती है। बहिष्करणीय सामाजिक-आर्थिक प्रवृत्तियों की ओर संकेत कर रहे हैं।
श्रम बाजार का परिदृश्य आधुनिक विचारों के साथ तेजी से बदल रहा है, जिसमें समुदायों में बदलाव हो रहा है, जो व्यवहार संबंधी बदलाव ला रहा है। अधिक मुस्लिम लड़कियां / महिलाएं स्कूलों और कॉलेजों के साथ-साथ श्रम बाजार में प्रवेश कर रही हैं। तथ्य यह है कि शिक्षित मुस्लिम महिलाएं बहुत अधिक बेरोजगारी दर की रिपोर्ट करती हैं, एक प्रमाण है कि सामाजिक मानदंडों को शिथिल किया गया है, जिससे उनमें से कई को और अधिक काम करने की अनुमति मिलती है, जो श्रम बाजार की क्षमता को अवशोषित करने की क्षमता से अधिक है।
ऐतिहासिक रूप से, मुसलमानों ने अन्य समुदायों की तुलना में शिक्षा में बदतर प्रदर्शन किया है। विभाजन के पूर्व दिनों में, उनकी साक्षरता दर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की तुलना में अधिक थी। विभाजन के दौरान यह बदल गया क्योंकि कई शिक्षित मुसलमानों ने पाकिस्तान जाने का विकल्प चुना। पिछले सात दशकों में, मुस्लिम साक्षरता में सुस्त वृद्धि हुई है। पिछले दशकों के दौरान, SC / ST आरक्षण और छात्रवृत्ति के कारण लाभान्वित हुए हैं। मुसलमानों को यह फायदा नहीं हुआ।
– अमिताभ कुंडू